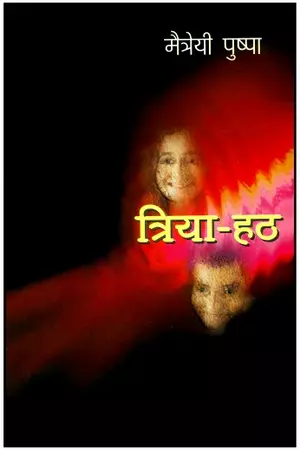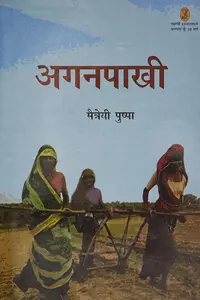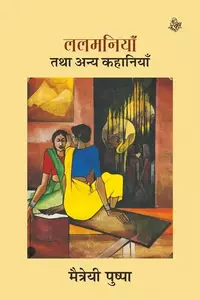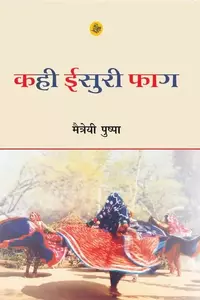|
नारी विमर्श >> त्रिया हठ त्रिया हठमैत्रेयी पुष्पा
|
236 पाठक हैं |
|||||||
यह पुस्तक पात्रों के खरे और खोटेपन की कहानी का वर्णन करता है...
Triya Hath
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘बेतवा बहती रही’ पुस्तक को पाठकों ने सराहा। उसके प्रत्याशित अंत पर बहुत सी स्त्रियाँ मुग्ध गई और रो पड़ी। फोन आए, पत्र आए। हम आपस मे संगति बिठाते हुए एक एक नजर आए। आप मानें या न मानें, मगर यही कहना ही प्रभावहीन हो गई। विगलन और आँसुओं में वह ताकत कहाँ, जो कथा को सफल ही नहीं, सार्थक भी बना दे। इसी आधार पर ‘बेतवा बहती रही’ पढ़िए और तब तक कि प्रस्तुत पुस्तक में आए पात्रों से जुड़ी यह दूसरी कहानी न पढ़ लें। यह मैं इस लिए कह रही हूँ कि मेरी करुणाजनित कथा-क्रंदन-भरी पुस्तक के बारे में आप सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं, जिसने अपनी विस्तारवादी प्रकृति से वास्तविकता और गप्प के अंतर को मिटा डाला। लेकिन गल्प ही तो ऐसा सशक्त साधन है, जो वास्तविकता का सच्चा भरोसा देता चलता है।
आज का युवा समीक्षक कहता है ‘कथानक और कथ्य का साँचा घिसा हुआ हो तो अच्छी या सार्थक कहानी की संभावना पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।’ इसी वाक्य की रोशनी में मैं अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करती हूँ और उन पात्रों के लिए कसौटी बनाती हूँ, जो ‘बेतवा बहती रही’ उपन्यास में आए हैं। ‘त्रिजा-हठ’ उन्हीं पात्रों के खरे और खोटेपन की कहानी है।
आज का युवा समीक्षक कहता है ‘कथानक और कथ्य का साँचा घिसा हुआ हो तो अच्छी या सार्थक कहानी की संभावना पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।’ इसी वाक्य की रोशनी में मैं अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करती हूँ और उन पात्रों के लिए कसौटी बनाती हूँ, जो ‘बेतवा बहती रही’ उपन्यास में आए हैं। ‘त्रिजा-हठ’ उन्हीं पात्रों के खरे और खोटेपन की कहानी है।
खामोशी के बारह वर्ष
मैंने अपनी कलम फिर उठा ली। बारह वर्ष बाद। मेरा अपना उपन्यास ‘बेतवा बहती रही’ ही कलम के दायरे में है। जिस समय मैंने यह रचना साहित्य-जगत् में सुधी पाठकों/समीक्षकों को सौंपी, उस वक्त उसके मुकम्मल होने के प्रति मैं आश्वस्त-सी थी या नहीं थी, निश्चित रूप से तय नहीं कर सकी, मगर मेरी प्रकृति पर तब शांति और संतोष की छाया-सी जरूर थी।
जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरे सामने यह सत्य उजागर होता गया कि जिस प्रकार कृति की रचनात्मकता अपनी निर्मित में अनेक साल लगा देती है, उसी तरह रचना का मर्म खुलने में अच्छा-खासा समय लगता है। कहानी की सार्थकता, जो कि लेखक का कथा-लक्ष्य होता है, उसमें बहुत-से खतरे-भरे बदलावों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उस परिवर्तन की प्रक्रिया से संगति बिठाना ही जीवन की नई निर्मिति प्रस्तुत करता है।
स्त्रियाँ अकसर ही खतरों से बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। कलाकार/रचनाकर के रूप में भी यही मानकर चलती हैं कि हामारा समाज किसी अप्रत्याशित सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहेगा। जिंदगी के फलक पर अपनी वास्तविकता में जब कभी अनहोना सत्य प्रकट होता है तो उसे निश्चित ही मनुष्य द्वारा घटित नहीं, भाग्य और ईश्वर का किया मान लिया जाता है, जिस पर कोई ऐतराज नहीं हो सकता है और न उसे किसी मानवीय तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। यही कारण है कि स्त्रियों के लेखन में ‘अप्रत्याशित सत्य’ की कौंध अकसर आते-आते रह जाती है। यथार्थ के अंतर्विरोध से निकला अयथार्थ आदर्श की चमकीली धुंध से घिर जाता है।
स्त्रियों का आदर्श, माने परिवार के लिए वह भयंकर त्याग, जिसमें नैसर्गिक भावनाओं का गला घोंट दिया जाए और मर्यादा निभाने का अविवेकी फैसला ही सर्वोपरी रहे। फिर आश्चर्य नहीं कि आज भी स्त्री-लेखन प्रेमचंद से पीछे है, जिनके घीसू-माधव (कफन) तो अप्रत्याशित आचरण करते हुए उच्छृंखल और अमर्यादित होते हुए जिंदगी में आनंद की खोज कर लेते हैं और उनके अमान्य व्यवहार असमान्य होते हुए यथास्थिति को चुनौती देते हैं। एक भीषण बदलाव की आहट समाज के अभेद्य किले पर उनकी दस्तक सुनाई देती है।....लेकिन उनके घर की स्त्री बधिया ? युवा बहू ? वह तो दर्दनाक स्थितियों में पीड़ा झेलती हुई आखिरकार लाश में चुपचाप तब्दील हो जाने के नियम को निभाती है कि किसी परिवर्तन का खटका तक न हो। यह वही मंजर है, जब अनुभव की प्रामाणिकता में स्त्री अपने चरित्रगत उत्थान को पति के घर और घेरे में सीमित कर लेती है, क्योंकि किसी तरह का प्रतिवाद उसके बदचलन होने के खतरे पैदा करता है। वह जानती है कि चरित्रहीन (यौनशुचिता को खंडित करने वाली) स्त्री का गुजारा सवर्ण समाजों में ही नहीं, हाशिये के समुदायों और दलित-वर्ग में भी नहीं है। पुरुषों की बिना आज्ञा या अनुमति के ‘घर के बाहर पाँव रखना’ भी एक अनेहोनी सच्चाई है।
‘बेतवा बहती रही’ पुस्तक को पाठकों ने सराहा। उसके प्रत्याशित अंत पर बहुत-सी स्त्रियाँ मुग्ध हुईं और रो पड़ी। फोन आए, पत्र आए। हम आपस में संगति बिठाते हुए एकमएक नजर आए। आप मानें या न मानें, मगर यही कहना ही प्रभावहीन हो गई। विगलन और आँसुओं में वह ताकत कहाँ, जो कथा को सफल ही नहीं, सार्थक भी बना दे। इसी आधार पर ‘बेतवा बहती रही’ पढ़िए और तब तक कि प्रस्तुत पुस्तक में आए पात्रों से जुड़ी यह दूसरी कहानी न पढ़ लें। यह मैं इस लिए कह रही हूँ कि मेरी करुणाजनित कथा-क्रंदन-भरी पुस्तक के बारे में आप सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं, जिसने अपनी विस्तारवादी प्रकृति से वास्तविकता और गप्प के अंतर को मिटा डाला। लेकिन गल्प ही तो ऐसा सशक्त साधन है, जो वास्तविकता का सच्चा भरोसा देता चलता है।
आज का युवा समीक्षक कहता है- ‘कथानक और कथ्य का साँचा घिसा हुआ हो तो अच्छी या सार्थक कहानी की संभावना पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।’ -यह वाक्य ‘कथादेश’ पत्रिका में ‘कहानी की उपस्थिति’ नामक स्तंभ को लिखने वाले समीक्षक जयप्रकाश का है। इसी वाक्य की रोशनी में मैं अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करती हूँ और उन पात्रों के लिए कसौटी बनाती हूँ, जो ‘बेतवा बहती रही’ उपन्यास में आए हैं। सबसे पहले पाती हूँ कि मैं क्या उन्हीं स्थितियों या मन: स्थितियों में थी, जिनके कारण नायिका का चरित्र गरिमामय दयनीयता का शिकार हुआ ? या मैंने खुद को सभ्य, आधुनिक और शहरी मानते हुए ग्रामीण स्त्री की जिंदगी का शोक-भरा मखौल उड़ाया ? अथवा यह हुआ कि मैं सर्वज्ञ की भूमिका निभाती हुई, संस्कार-पीड़ित की तरह सामाजिक दबावों से लड़ नहीं सकी। जस की तस, राई-भर अयथार्थ का तत्व नहीं मिला पाई कि कहीं मान्यताओं का सौंदर्य बिगड़ न जाए। मुझे रचना अपने नाम के साथ जो पेश करनी थी। -मैं क्या वही नहीं थी, जो यह कहती देखी-पढ़ी जा सकती हैं कि ‘स्त्री देह से संबंधित सरोकार उनका विषय नहीं-मेरे संबंध अगर अन्य पुरुष से होते हुए भी तो एक मेरा परिवार है, संसार है। मुझे अपने लेखन को ऐसे रखना है, जिसे घर के लोग शालीनता से पढ़ सकें (मैं अशालीनता का खतरा नहीं उठाना चाहती)।’
अत: मैं कहानी को समाज के नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दे रही थी। मैं भी घर में सुरक्षित-साबुत रही। सोने पर सुहागा देखिए कि ज्यादातर साहित्यिक प्रतिक्रियाओं ने मुझे निराश नहीं किया। आज सोचती हूँ, क्या जनवाद के पैरोकार स्त्री-चरित्रों को लेकर उतना आग्रह नहीं रखते, जितना कि मजदूरों को लेकर रखते हैं ? क्या उन्हें औरत का जीवन ‘बेगारी’ होने के लिए मान्य है ? इस विषय पर भोलेपन और मानसिक शांति की बराबर मात्रा लोगों को बड़ा आनंद देती है। और हाँ, वे स्त्री की संघर्ष-यात्रा में किसी मंजिल का पता नहीं चाहते, यह मैंने ‘अल्मा कबूतरी’ (उपन्यास) लिखने के बाद जाना। जिस लक्ष्य-प्राप्ति के कारण अल्मा आँख का काँटा बन गई, उसके बरअक्स मृत्यु को वरण करनेवाली पतिव्रता उर्वशी काँटा बनने से बच गई और मैं लेखिका के रूप में काँटा में उलझने से रह गई।
मगर तभी एक मासूम-से सवाल ने मेरे आसपास आहट की।
एक लड़के ने पास आकर मेरी आखों में देखा।
‘‘क्या देख रहे हो ?’’
‘‘यही कि आपकी आँखों में कितना पानी बचा है ?’’
‘मासूम’- यह शब्द बड़ा कठोर है। मैंने देवेश (उर्वशी का बेटा) को देखकर समझा कि न आज के युवा मासूम हैं, न उनके सवाल भोले।
उर्वशी के बेटे देवेश की तरह तमाम युवक बड़े हो रहे हैं और वे परिश्रम के पसीने में नहाए उन भीरु किसानों, किसान-पत्नियों के जीवन को परिवर्तन के संधान के रूप में देखना चाहते हैं, यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई। तब तो मैंने यही समझा था कि अपने कुल-खानदान की कथा उघाड़ने के लिए यह युवक मुझसे माफीनामे की उम्मीद बाँधकर आया है। और मेरे लिए अब यह नकारात्मक रुख नया नहीं रहा। आसपास तमाम ऊँची बाधाएँ मैं आमने-सामने पड़कर देख सकती हूँ।
‘‘आपने अपनी कथा को यह रूप दिया मीरा जिज्जी ?’’
‘‘मैं मीरा जिज्जी हूँ ? हूँ क्या ?’’
‘‘किताब के साँचे-ढले दृश्य मुझे परेशान करते हैं।’’ देवेश ने अपनी बात कही।
और अब देवेश जैसी उम्र के तमाम पाठक सामने आ गए।
‘‘देखिए, अब ‘बूढ़े से नवयुवती का विवाह’-यह समस्या प्रमुख नहीं है। हाँ, लड़की बेचने, दहेज देने और दहेज-हत्याओं का सवाल भयावह है। समाज में तेजी से फैलता हुआ और नतीजे में भ्रूण-हत्या से गुजरता हुआ।’’ देवेश ने यह बात कहते समय चेहरे पर आते-जाते भावों से दरसा दिया कि मैं स्त्री के जिस त्याग को महत्त्वपूर्ण माने बैठी हूँ, वही कहानी के महत्वपूर्ण पक्ष को क्षरित कर रहा है। उसने कहा, ‘‘आप बहुत पीछे रह गई हैं। ऐसे ही, जैसे आपके समकालीन लेखक पुराने कथा-फ़ार्मूले में जकड़े हुए हैं।’’
‘‘कैसे ?’’ मैंने पूछा।
‘‘मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं। नए से नया लेखक जब साप्रदायिकता को विषय बनाकर कहानी लिखता है या उपन्यास की रचना करता है, तो अभिंव्यक्ति में उसकी अनुगूँज 1948 में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बँटवारे पर लिखी कथाओं की गूँजों से अलग नहीं होती। एक हिन्दू लड़का, एक मुस्लिम लड़की-दोनों का किस्सा हमारे गाँव की वृद्धाएँ अपने गुजरे जमाने का गीत बताकर हमें सुनाती रही हैं। आप भी सुन लें तो अच्छा रहे।’’
मैं गौर से उसे देखती हूँ। वह मुस्करा देता है।
वह बूढ़ी दादी-काकियों के गीत को कविता की तरह सुनाता है :
जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरे सामने यह सत्य उजागर होता गया कि जिस प्रकार कृति की रचनात्मकता अपनी निर्मित में अनेक साल लगा देती है, उसी तरह रचना का मर्म खुलने में अच्छा-खासा समय लगता है। कहानी की सार्थकता, जो कि लेखक का कथा-लक्ष्य होता है, उसमें बहुत-से खतरे-भरे बदलावों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उस परिवर्तन की प्रक्रिया से संगति बिठाना ही जीवन की नई निर्मिति प्रस्तुत करता है।
स्त्रियाँ अकसर ही खतरों से बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। कलाकार/रचनाकर के रूप में भी यही मानकर चलती हैं कि हामारा समाज किसी अप्रत्याशित सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहेगा। जिंदगी के फलक पर अपनी वास्तविकता में जब कभी अनहोना सत्य प्रकट होता है तो उसे निश्चित ही मनुष्य द्वारा घटित नहीं, भाग्य और ईश्वर का किया मान लिया जाता है, जिस पर कोई ऐतराज नहीं हो सकता है और न उसे किसी मानवीय तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। यही कारण है कि स्त्रियों के लेखन में ‘अप्रत्याशित सत्य’ की कौंध अकसर आते-आते रह जाती है। यथार्थ के अंतर्विरोध से निकला अयथार्थ आदर्श की चमकीली धुंध से घिर जाता है।
स्त्रियों का आदर्श, माने परिवार के लिए वह भयंकर त्याग, जिसमें नैसर्गिक भावनाओं का गला घोंट दिया जाए और मर्यादा निभाने का अविवेकी फैसला ही सर्वोपरी रहे। फिर आश्चर्य नहीं कि आज भी स्त्री-लेखन प्रेमचंद से पीछे है, जिनके घीसू-माधव (कफन) तो अप्रत्याशित आचरण करते हुए उच्छृंखल और अमर्यादित होते हुए जिंदगी में आनंद की खोज कर लेते हैं और उनके अमान्य व्यवहार असमान्य होते हुए यथास्थिति को चुनौती देते हैं। एक भीषण बदलाव की आहट समाज के अभेद्य किले पर उनकी दस्तक सुनाई देती है।....लेकिन उनके घर की स्त्री बधिया ? युवा बहू ? वह तो दर्दनाक स्थितियों में पीड़ा झेलती हुई आखिरकार लाश में चुपचाप तब्दील हो जाने के नियम को निभाती है कि किसी परिवर्तन का खटका तक न हो। यह वही मंजर है, जब अनुभव की प्रामाणिकता में स्त्री अपने चरित्रगत उत्थान को पति के घर और घेरे में सीमित कर लेती है, क्योंकि किसी तरह का प्रतिवाद उसके बदचलन होने के खतरे पैदा करता है। वह जानती है कि चरित्रहीन (यौनशुचिता को खंडित करने वाली) स्त्री का गुजारा सवर्ण समाजों में ही नहीं, हाशिये के समुदायों और दलित-वर्ग में भी नहीं है। पुरुषों की बिना आज्ञा या अनुमति के ‘घर के बाहर पाँव रखना’ भी एक अनेहोनी सच्चाई है।
‘बेतवा बहती रही’ पुस्तक को पाठकों ने सराहा। उसके प्रत्याशित अंत पर बहुत-सी स्त्रियाँ मुग्ध हुईं और रो पड़ी। फोन आए, पत्र आए। हम आपस में संगति बिठाते हुए एकमएक नजर आए। आप मानें या न मानें, मगर यही कहना ही प्रभावहीन हो गई। विगलन और आँसुओं में वह ताकत कहाँ, जो कथा को सफल ही नहीं, सार्थक भी बना दे। इसी आधार पर ‘बेतवा बहती रही’ पढ़िए और तब तक कि प्रस्तुत पुस्तक में आए पात्रों से जुड़ी यह दूसरी कहानी न पढ़ लें। यह मैं इस लिए कह रही हूँ कि मेरी करुणाजनित कथा-क्रंदन-भरी पुस्तक के बारे में आप सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं, जिसने अपनी विस्तारवादी प्रकृति से वास्तविकता और गप्प के अंतर को मिटा डाला। लेकिन गल्प ही तो ऐसा सशक्त साधन है, जो वास्तविकता का सच्चा भरोसा देता चलता है।
आज का युवा समीक्षक कहता है- ‘कथानक और कथ्य का साँचा घिसा हुआ हो तो अच्छी या सार्थक कहानी की संभावना पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।’ -यह वाक्य ‘कथादेश’ पत्रिका में ‘कहानी की उपस्थिति’ नामक स्तंभ को लिखने वाले समीक्षक जयप्रकाश का है। इसी वाक्य की रोशनी में मैं अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करती हूँ और उन पात्रों के लिए कसौटी बनाती हूँ, जो ‘बेतवा बहती रही’ उपन्यास में आए हैं। सबसे पहले पाती हूँ कि मैं क्या उन्हीं स्थितियों या मन: स्थितियों में थी, जिनके कारण नायिका का चरित्र गरिमामय दयनीयता का शिकार हुआ ? या मैंने खुद को सभ्य, आधुनिक और शहरी मानते हुए ग्रामीण स्त्री की जिंदगी का शोक-भरा मखौल उड़ाया ? अथवा यह हुआ कि मैं सर्वज्ञ की भूमिका निभाती हुई, संस्कार-पीड़ित की तरह सामाजिक दबावों से लड़ नहीं सकी। जस की तस, राई-भर अयथार्थ का तत्व नहीं मिला पाई कि कहीं मान्यताओं का सौंदर्य बिगड़ न जाए। मुझे रचना अपने नाम के साथ जो पेश करनी थी। -मैं क्या वही नहीं थी, जो यह कहती देखी-पढ़ी जा सकती हैं कि ‘स्त्री देह से संबंधित सरोकार उनका विषय नहीं-मेरे संबंध अगर अन्य पुरुष से होते हुए भी तो एक मेरा परिवार है, संसार है। मुझे अपने लेखन को ऐसे रखना है, जिसे घर के लोग शालीनता से पढ़ सकें (मैं अशालीनता का खतरा नहीं उठाना चाहती)।’
अत: मैं कहानी को समाज के नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दे रही थी। मैं भी घर में सुरक्षित-साबुत रही। सोने पर सुहागा देखिए कि ज्यादातर साहित्यिक प्रतिक्रियाओं ने मुझे निराश नहीं किया। आज सोचती हूँ, क्या जनवाद के पैरोकार स्त्री-चरित्रों को लेकर उतना आग्रह नहीं रखते, जितना कि मजदूरों को लेकर रखते हैं ? क्या उन्हें औरत का जीवन ‘बेगारी’ होने के लिए मान्य है ? इस विषय पर भोलेपन और मानसिक शांति की बराबर मात्रा लोगों को बड़ा आनंद देती है। और हाँ, वे स्त्री की संघर्ष-यात्रा में किसी मंजिल का पता नहीं चाहते, यह मैंने ‘अल्मा कबूतरी’ (उपन्यास) लिखने के बाद जाना। जिस लक्ष्य-प्राप्ति के कारण अल्मा आँख का काँटा बन गई, उसके बरअक्स मृत्यु को वरण करनेवाली पतिव्रता उर्वशी काँटा बनने से बच गई और मैं लेखिका के रूप में काँटा में उलझने से रह गई।
मगर तभी एक मासूम-से सवाल ने मेरे आसपास आहट की।
एक लड़के ने पास आकर मेरी आखों में देखा।
‘‘क्या देख रहे हो ?’’
‘‘यही कि आपकी आँखों में कितना पानी बचा है ?’’
‘मासूम’- यह शब्द बड़ा कठोर है। मैंने देवेश (उर्वशी का बेटा) को देखकर समझा कि न आज के युवा मासूम हैं, न उनके सवाल भोले।
उर्वशी के बेटे देवेश की तरह तमाम युवक बड़े हो रहे हैं और वे परिश्रम के पसीने में नहाए उन भीरु किसानों, किसान-पत्नियों के जीवन को परिवर्तन के संधान के रूप में देखना चाहते हैं, यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई। तब तो मैंने यही समझा था कि अपने कुल-खानदान की कथा उघाड़ने के लिए यह युवक मुझसे माफीनामे की उम्मीद बाँधकर आया है। और मेरे लिए अब यह नकारात्मक रुख नया नहीं रहा। आसपास तमाम ऊँची बाधाएँ मैं आमने-सामने पड़कर देख सकती हूँ।
‘‘आपने अपनी कथा को यह रूप दिया मीरा जिज्जी ?’’
‘‘मैं मीरा जिज्जी हूँ ? हूँ क्या ?’’
‘‘किताब के साँचे-ढले दृश्य मुझे परेशान करते हैं।’’ देवेश ने अपनी बात कही।
और अब देवेश जैसी उम्र के तमाम पाठक सामने आ गए।
‘‘देखिए, अब ‘बूढ़े से नवयुवती का विवाह’-यह समस्या प्रमुख नहीं है। हाँ, लड़की बेचने, दहेज देने और दहेज-हत्याओं का सवाल भयावह है। समाज में तेजी से फैलता हुआ और नतीजे में भ्रूण-हत्या से गुजरता हुआ।’’ देवेश ने यह बात कहते समय चेहरे पर आते-जाते भावों से दरसा दिया कि मैं स्त्री के जिस त्याग को महत्त्वपूर्ण माने बैठी हूँ, वही कहानी के महत्वपूर्ण पक्ष को क्षरित कर रहा है। उसने कहा, ‘‘आप बहुत पीछे रह गई हैं। ऐसे ही, जैसे आपके समकालीन लेखक पुराने कथा-फ़ार्मूले में जकड़े हुए हैं।’’
‘‘कैसे ?’’ मैंने पूछा।
‘‘मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं। नए से नया लेखक जब साप्रदायिकता को विषय बनाकर कहानी लिखता है या उपन्यास की रचना करता है, तो अभिंव्यक्ति में उसकी अनुगूँज 1948 में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बँटवारे पर लिखी कथाओं की गूँजों से अलग नहीं होती। एक हिन्दू लड़का, एक मुस्लिम लड़की-दोनों का किस्सा हमारे गाँव की वृद्धाएँ अपने गुजरे जमाने का गीत बताकर हमें सुनाती रही हैं। आप भी सुन लें तो अच्छा रहे।’’
मैं गौर से उसे देखती हूँ। वह मुस्करा देता है।
वह बूढ़ी दादी-काकियों के गीत को कविता की तरह सुनाता है :
‘‘स्टेशन पर बैठी छोरी मुसलमान की
बाबूजी, मेरी टिकट काट दो पाकिस्तान की
एक लाखा, एक चूड़ा घर से ले आऊँगा
मैं बनिये का लाल तेरी जान बचाऊँगा
पर बमान की न बनिये की, लड़की शेख पठान की
बाबूजी, मेरी टिकट काट दो पाकिस्तान की
एक लाखा, एक चूड़ा घर से ले आऊँगा
मैं बनिये का लाल तेरी जान बचाऊँगा
पर बमान की न बनिये की, लड़की शेख पठान की
बाबूजी, मेरी टिकट काट दो पाकिस्तान की.....।’’
‘‘सत्तावन साल गुजर गए इस गीत को बने हुए। कहानी नहीं बदली बिल्कुल भी, क्योंकि रचना के फलक पर आज भी बामन, बनिये, ठाकुर, कायस्थों के लाल मुसलमान लड़कियों को सुरक्षा का वादा दे रहे हैं। जैसे मसीहाई हिन्दुओं की ही विरासत हो। साथ ही उस स्त्री को अपनी वर्ग-चेतना के रूबरू खड़ा नहीं होने देते, वरन् मुसलमान लड़की भी रक्षा-सुरक्षा देने में आगे आई होती। आप तो खुद स्त्री हो, क्या उधार की सुरक्षा की कायल हो ? उधार की सुरक्षा अकसर धोखा देती है, जैसे कि.....।’’
‘‘जैसे कि......मतलब ?’’ मैं पूछती हूँ।
वह मेरी ओर न देखकर धूप को देखते हुए मुस्कराया।
‘‘अपना पक्ष रखो न ! हम भी तो देखें, तुम किस अप्रत्याशित के इंतजार में हो। तुम तो देवेश, पानी के आग हो जाने की संभावनाएँ देख रहे हो। मगर समझकर रखो कि पानी का स्वभाव पानी ही होता है, उबलने के बाद लगातार ठंडा होते जाना। स्त्री का स्वभाव भी तो इससे अलग तो नहीं।’’
वह ठंडी साँस लेकर रह गया। दो क्षण बाद बोला- ‘‘ठीक है आपकी बात, पर पानी का स्वभाव कीचड़ हो जाना भी नहीं होता। लोग उसे कीचड़ कर देते हैं।’’
‘‘सत्तावन साल गुजर गए इस गीत को बने हुए। कहानी नहीं बदली बिल्कुल भी, क्योंकि रचना के फलक पर आज भी बामन, बनिये, ठाकुर, कायस्थों के लाल मुसलमान लड़कियों को सुरक्षा का वादा दे रहे हैं। जैसे मसीहाई हिन्दुओं की ही विरासत हो। साथ ही उस स्त्री को अपनी वर्ग-चेतना के रूबरू खड़ा नहीं होने देते, वरन् मुसलमान लड़की भी रक्षा-सुरक्षा देने में आगे आई होती। आप तो खुद स्त्री हो, क्या उधार की सुरक्षा की कायल हो ? उधार की सुरक्षा अकसर धोखा देती है, जैसे कि.....।’’
‘‘जैसे कि......मतलब ?’’ मैं पूछती हूँ।
वह मेरी ओर न देखकर धूप को देखते हुए मुस्कराया।
‘‘अपना पक्ष रखो न ! हम भी तो देखें, तुम किस अप्रत्याशित के इंतजार में हो। तुम तो देवेश, पानी के आग हो जाने की संभावनाएँ देख रहे हो। मगर समझकर रखो कि पानी का स्वभाव पानी ही होता है, उबलने के बाद लगातार ठंडा होते जाना। स्त्री का स्वभाव भी तो इससे अलग तो नहीं।’’
वह ठंडी साँस लेकर रह गया। दो क्षण बाद बोला- ‘‘ठीक है आपकी बात, पर पानी का स्वभाव कीचड़ हो जाना भी नहीं होता। लोग उसे कीचड़ कर देते हैं।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book